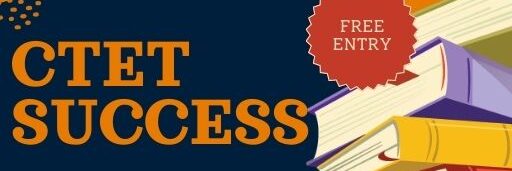संज्ञान Cognition
बालों में संज्ञानात्मक विकास Cognitive Development in Children
- संवेदी-गतिक अवस्था (जन्म से 2 वर्ष)
- पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था (2 से 7 वर्ष)
- प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था (7 से 11 वर्ष)
- औपचारिक-संक्रियात्मक अवस्था (11 + वर्ष)
प्रारम्भिक बाल्यकाल (2 से 6 वर्ष) में संज्ञानात्मक विकास Cognitive Development in Infancy (2 to 6 Years)
- इस काल में बच्चे, शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं के प्रयोग में अधिक प्रवीण हो जाते हैं।
- स्कूल जाने तक बच्चों की शब्दावली पर्याप्त अच्छी हो जाती है। वास्तव में बच्चे विभिन्न सन्दर्भों में अन्य भाषाएँ सीखने में अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। अनेक बार वे द्विभाषी या बहुभाषी के रूप में विकसित होते हैं। वे एक भाषी बच्चों की अपेक्षा भाषा की अच्छी समझ वाले होते हैं।
- प्रारम्भिक बाल्यकाल में स्थायी अवधान में वृद्धि हो जाती है। एक 3 वर्ष का बच्चा चित्रांकनी से रंग भरने, खिलौने से खेलने या 15-20 मिनट तक टेलीविजन देखने की जिद कर सकता है। इसके विपरीत एक 6 वर्ष का बच्चा किसी रोचक कार्य पर एक घण्टे से अधिक कार्य करता देखा जा सकता है।
- बच्चे अपने संविधान में अधिक चयनात्मक हो जाते हैं। परिणामस्वरूप उनके प्रत्यक्षात्मक कौशल भी उन्नत होते हैं।
- चिन्तन और अधिक तर्कपूर्ण हो जाता है और याद रखने की क्षमता और जानकारी की प्रक्रिया भी उन्नत होती है। वातावरण से अन्तःक्रिया द्वारा बच्चा सामाजिक व्यवहार के सही नियम सीखता है जो उसे विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं।
- प्रारम्भिक बाल्यकाल, 2 से 6 वर्ष में बच्चा पूर्व क्रियात्मक अवस्था द्वारा प्रगति करता है।
पूर्व-क्रियात्मक अवस्था की 2 उप-अवस्थाएँ होती हैं :-
- प्रतीकात्मक क्रिया, उप-अवस्था में, बच्चे वस्तुओं का मानसिक प्रतिबिम्ब बना लेते हैं और उसे बाद में उपयोग करने के लिए सम्भाल कर रख लेते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा एक छोटे कुत्ते की आकृति बनाए या उससे खेलने का नाटक करे, जोकि वहाँ उपस्थित ही नहीं है। बालक उन लोगों के विषय में बात कर सकते हैं जो यात्रा कर रहे हैं या जो कहीं अन्य स्थान पर रहते हों। वे उन स्थानों का भी रेखाचित्र बना सकते हैं, जो उन्होंने देखे हैं, साथ ही साथ अपनी कल्पना से नये दृश्य और जीव भी बना सकते हैं।
- बच्चे अपनी वस्तुओं के मानसिक प्रतिबिम्ब का भी खेल में भूमिका निभाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
मध्य बाल्यकाल में संज्ञानात्मक विकास Cognitive Development in Childhood
- तार्किक नियमों को समझना।
- स्थानिक तर्क में सधार।
- तार्किक चिंतन, यथार्थ और इन्द्रियगोचर स्थितियों तक सीमित।
संवेग Emotion
संवेग’ अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिन्दी रूपान्तरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ‘इमोवेयर’ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ‘उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग’ को व्यक्ति की ‘उत्तेजित दशा’ कहते हैं। इस प्रकार संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है।
- मनुष्य अपनी रोजाना की जिन्दगी में सुख, दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है।
- वुडवर्थ के अनुसार “संवेग, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है।”
- ड्रेवर के अनुसार “संवेग, प्राणी की एक जटिल दशा है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है”।
- जे.एस.रॉस के अनुसार “संवेग, चेतना की वह अवस्था है, जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है।”
- जरशील्ड के अनुसार “किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं।”
सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे समाज के निर्माण लैंगिक मुद्दे और परेशानियों को समझने क लिए लिंक माध्यम से अध्ययन कीजिये। इस टॉपिक से प्रायः 3 से 6 प्रश्न पूछे जाते है।
संवेग के प्रकार Types of Emotion
संवेगों का सम्बन्ध मूल प्रवृत्तियों से होता है। चौदह मूल प्रवृत्तियों के चौदह ही संवेग के हैं, जो इस प्रकार है :-
- भय
- वात्सल्य
- घृणा
- कामुकता
- करुणा व दुःख
- आत्महीनता
- आत्माभिमान
- अधिकार भावना
- भूख
- आमोद
- कृतिभाव
- आश्चर्य
- एकाकीपन
संवेगों की प्रकृति Nature of Emotions
- हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं अनुभव करते हैं।
- संवेगों के उदाहरण हैं खुश होना, शर्मिन्दा होना, दुःखी होना, उदास होना आदि।
- संवेग हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं।
संवेगों के घटक Factors/Components of Emotions
शारीरिक परिवर्तन Physical Changes
जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तब उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जैसे- हृदय गति और रक्त चाप बढ़ जाना, पुतली का बड़ा हो जाना, साँस तेज होना, मुँह का रूखा हो जाना या पसीना निकलना आदि। सोचिए जब आप किसी परीक्षा केन्द्र गए थे और परीक्षा दी थी या जब आप अपने छोटे भाई से नाराज हुए थे, तब शायद आपने ये शारीरिक परिवर्तन अनुभव किए होंगे।
अधिगम | विकास के साथ अधिगम का सम्बन्ध
व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति Changes in Behaviour and Emotional Expression
इसका तात्पर्य बाहरी और ध्यान देने योग्य चिह्नों से है, जो एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। इसमें चेहरे के हाव-भाव, शारीरिक स्थिति, हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना, मुस्कुराना, क्रोध करना एवं कुर्सी पर धम्म से बैठना सम्मिलित हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति के छः मूल संवेग हैं भय, क्रोध, दुःख, आश्चर्य घृणा एवं प्रसन्नता। इसका तात्पर्य है कि यह संवेग विश्वभर के लोगों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं।
सर्वगात्मक भावना Emotional Feelings
संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हों। हम संवेग को वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे प्रसन्न, दुःखी, क्रोध, घृणा आदि। हमारे पूर्व अनुभव और संस्कृति जिससे हम जुड़े हुए हैं हमारी भावनाओं को आकृति प्रदान करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के हाथ में छड़ी देखते हैं, तो हम भाग सकते हैं या अपने आपको लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं, जब यदि एक प्रसिद्ध गायक आपके पड़ोस में रहता है, तो आप उससे अपने प्रिय गीत सुनने के लिए चले जाएँगे।
संवेगों का शिक्षा में महत्त्व Importance of Emotions in Education
- शिक्षक, बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके, उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों में उपयुक्त संवेगों को जाग्रत करके, उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है।
- शिक्षक, बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके, उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों को अपने संवेगों पर नियन्त्रण करने की विधियाँ बताकर, उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है।
- शिक्षक बालको के संवेगों का विकास करके, उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है।