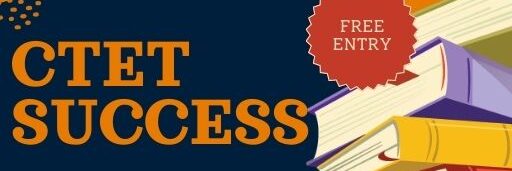Part – 2
सीखने के गौण नियम
Subordinate Laws of Learning
1. बहु-प्रतिक्रिया का नियम Law of Multiple Responses)
इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नई समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे सन्तोष मिलता है। असफल होने पर व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि एक के बाद एक उपाय पर अमल करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए। यह नियम ‘प्रयत्न एवं भूल’ पर आधारित है।
2. मानसिक स्थिति का नियम (Law of Mental Status)
इस नियम को तत्परता या अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। यह नियम इस बात पर बल देता है कि बाहरी स्थिति की ओर प्रतिक्रियाएँ व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती हैं अर्थात्, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नये कार्यो को आसानी से सीख लेगा और यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। निद्रा, सभ्यता, थकावट, आकाँक्षाएँ, भावनाएँ आदि सभी हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ मूर्ति को देखकर हिन्दू हाथ जोड़ लेते हैं, मूर्ति के सामने मस्तक टेककर सन्तुष्ट होते हैं और मूर्ति को चोट पहुंचाने से उन्हें भी चोट पहुँचती है।
3. आंशिक क्रिया का नियम (Law of Partial Function)
यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया सम्पूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है। यह केवल सम्पूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति ही होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती हैं। इस नियम में इस प्रकार ‘अंश से पूर्ण की ओर’ शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। पाठ योजना को छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाना इसी नियम पर आधारित है। संक्षेप में, व्यक्ति किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसके अनावश्यक विस्तार को छोड़कर उसके मूल तत्त्वों पर अपनी अनुक्रिया केन्द्रित कर लेता है। आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम बताया है।
4. समानता का नियम ( Law of Equality )
इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उससे मिलती-जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है, जिससे वह पहले भी गुजर चुका है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति नवीन परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसी उसने पुरानी परिस्थिति में की थी। समान तत्त्वों के आधार पर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बद्ध करके पढ़ाने से सीखना सरल हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर’ शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है।
5. साहचर्य परिवर्तन का नियम (Law of Associative Changing)
जैसा कि इस नियम के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक से जुड़ी हुई अथवा उसकी किसी सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। उदाहरणार्थं भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुँह से लार टपकने लगती है लेकिन कुछ समय बाद खाने के प्याले को देखकर ही लार टपकने लगती है। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित-अनुक्रिया को सहचारी स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है।